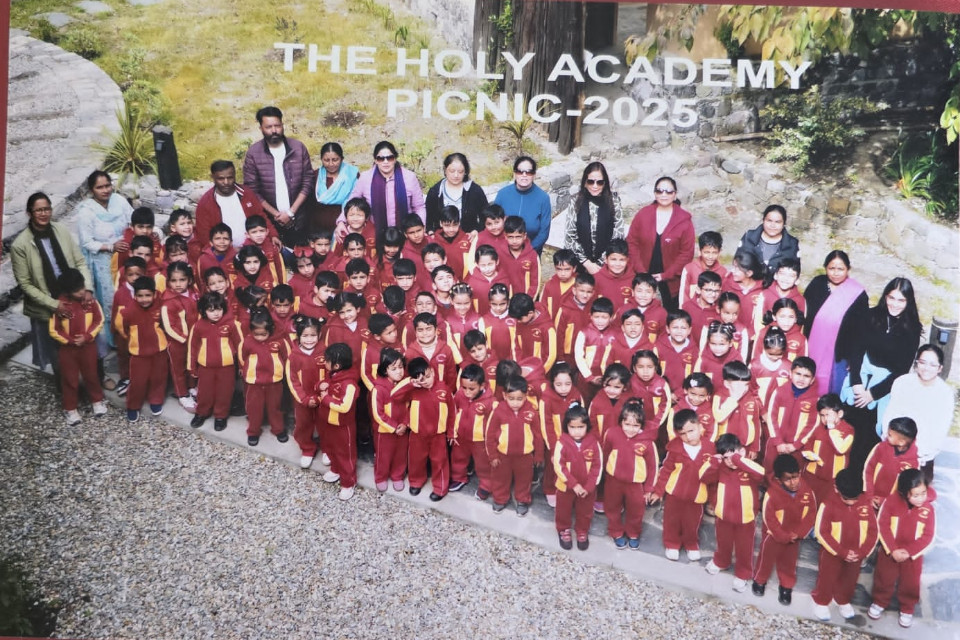शिक्षक दिवस: शिक्षा की गौरवमयी परंपरा से जुड़ा है भारत का इतिहास! व्यवसायीकरण और बाजारीकरण देश के समक्ष बड़ी चुनौती
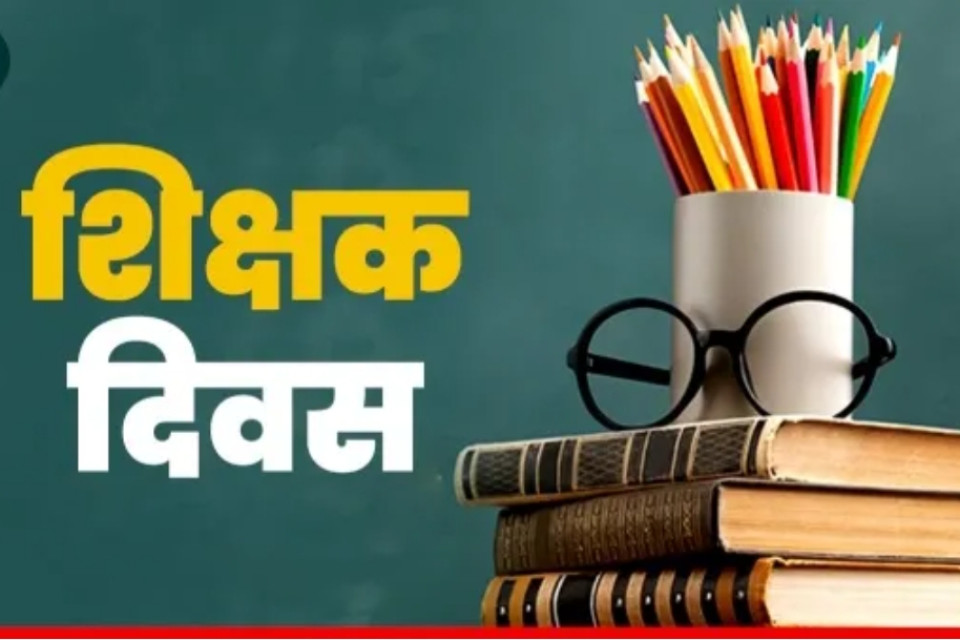
आज, 5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान गुरुजनों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को ही मनाने की वजह भी दिलचस्प है। दरअसल भारतीय शिक्षाविद, दार्शनिक और राजनेता रहे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था और उन्होंने कहा था कि उनका जन्मदिन अलग से न मनाकर, इसे शिक्षकों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाए। इसीलिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे भारतीय राष्ट्रपति थे। इस दिवस का उद्देश्य समाज में शिक्षक के महत्व, उनके योगदान और मार्गदर्शक भूमिका को सम्मान देना है। यह अवसर विद्यार्थियों और समाज को याद दिलाता है कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं बल्कि आदर्श, प्रेरक और चरित्र-निर्माता भी होते हैं। आज जबकि नया भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत निर्मित हो रहा है, तब शिक्षकों की भूमिका अधिक प्रासंगिक हो गयी है। बता दें कि भारत का इतिहास शिक्षा की गौरवमयी परंपरा से जुड़ा है। प्राचीन समय से भारत शिक्षा का बड़ा केन्द्र रहा है और उसने संसार में जगतगुरु की भूमिका निभाई है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने भारत को जगतगुरु का दर्जा दिलाया। महान् दार्शनिक आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा था-“व्यक्तित्व-निर्माण का कार्य अत्यन्त कठिन है और यह केवल निःस्वार्थी एवं जागरूक शिक्षक ही कर सकता है।” यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। प्राचीन भारतीय दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य ‘सा विद्या या विमुक्तये’ रहा है, अर्थात् शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह ‘सा विद्या या नियुक्तये’ बन गई है अर्थात् शिक्षा वही है जो नौकरी दिलाए। यही कारण है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने के बावजूद समाज में अपराध और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है-“एक स्कूल खुलेगा तो सौ जेलें बंद होंगी।” परन्तु आज स्थिति इसके विपरीत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया है। इसमें केवल क्या पढ़ना है पर ही नहीं, बल्कि कैसे पढ़ना है, इस पर भी जोर दिया गया है। आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, उद्यमशीलता और नैतिकता को शिक्षा के केंद्र में रखा गया है। लेकिन इन सभी का केन्द्रबिंदु शिक्षक ही है। यदि शिक्षक प्रेरणाहीन, निरुत्साहित या असंवेदनशील होंगे तो कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। शिक्षा केवल किताबों और पाठ्यक्रम से नहीं, बल्कि शिक्षक की जीवंत उपस्थिति से सार्थक होती है। पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था-“अगर कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त है और सुंदर दिमागों का राष्ट्र बन गया है, तो उसके लिए तीन प्रमुख व्यक्ति जिम्मेदार होंगे-पिता, माता और शिक्षक।” यह कथन शिक्षक के महत्व को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करता है। भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार होगा जब हमारे शिक्षक नई पीढ़ी को केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि चरित्रवान भी बनाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। नेल्सन मंडेला ने कहा था-“शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे दुनिया बदली जा सकती है।” युद्ध और आतंक के बीज मानव मस्तिष्क में जन्म लेते हैं, इसलिए बचपन से ही शांति और सह-अस्तित्व के बीज बोने होंगे। बच्चों को अपने देश से प्रेम के साथ विश्व-प्रेम यानी मानवता का पाठ सिखाना होगा, तभी दुनिया से युद्ध, हिंसा, आतंक का खात्मा होगा। भारतीय संस्कृति का “वसुधैव कुटुम्बकम्” मूल मंत्र इसमें सहायक बन सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का स्वरूप धीरे-धीरे मिशन से व्यवसाय की ओर झुकता जा रहा है। ज्ञान की बोली लग रही है, शिक्षक और छात्र के संबंधों में अविश्वास और हिंसा की खबरें बढ़ रही हैं। शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने और उसे मानवीय मूल्यों से जोड़ने की जिम्मेदारी सबसे पहले शिक्षकों पर ही आती है। आज आवश्यकता केवल शिक्षा क्रांति की नहीं, बल्कि शिक्षक क्रांति की भी है। अच्छे पाठ्यक्रम, नई तकनीक और आधुनिक संस्थानों की व्यवस्था तभी सार्थक है जब उनके केंद्र में ऐसे शिक्षक हों, जो छात्रों को प्रेरणा दें, जो उनके सर्वांगीण विकास का माध्यम बनें। खेत, बीज और उपकरण के रहते हुए किसान न हो तो सब बेकार है। उसी प्रकार, विद्यालय, पाठ्यक्रम और तकनीक के रहते हुए यदि शिक्षक नहीं हैं तो सब निरर्थक है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था-“सर्वांगीण विकास का अर्थ है हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म से महान।” शिक्षक ही ऐसे व्यक्तित्व गढ़ते हैं। शिक्षा के बदलते अर्थ ने समाज की मानसिकता को बदल दिया है। यही कारण है कि आज समाज में लोग केवल शिक्षित होना चाहते हैं, सुशिक्षित यानी गुण-सम्पन्न नहीं बनना चाहते। मानो उनका लक्ष्य केवल बौद्धिक विकास ही है। इन स्थितियों से शिक्षकों को बाहर निकलने में नई शिक्षा नीति से बहुत अपेक्षाएं हैं। आज के समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण देश के समक्ष बड़ी चुनौती हैं। पुराने समय में भारत में शिक्षा कभी व्यवसाय या धंधा नहीं थी। इससे छात्रों को बडी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। शिक्षक ही भारत देश को शिक्षा के व्यवसायीकरण और बाजारीकरण से स्वतंत्र कर सकते हैं। देश के शिक्षक ही पथ प्रदर्शक बनकर भारत में शिक्षा जगत को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं।