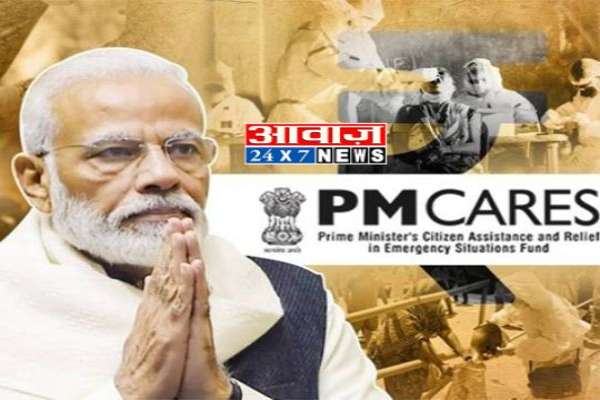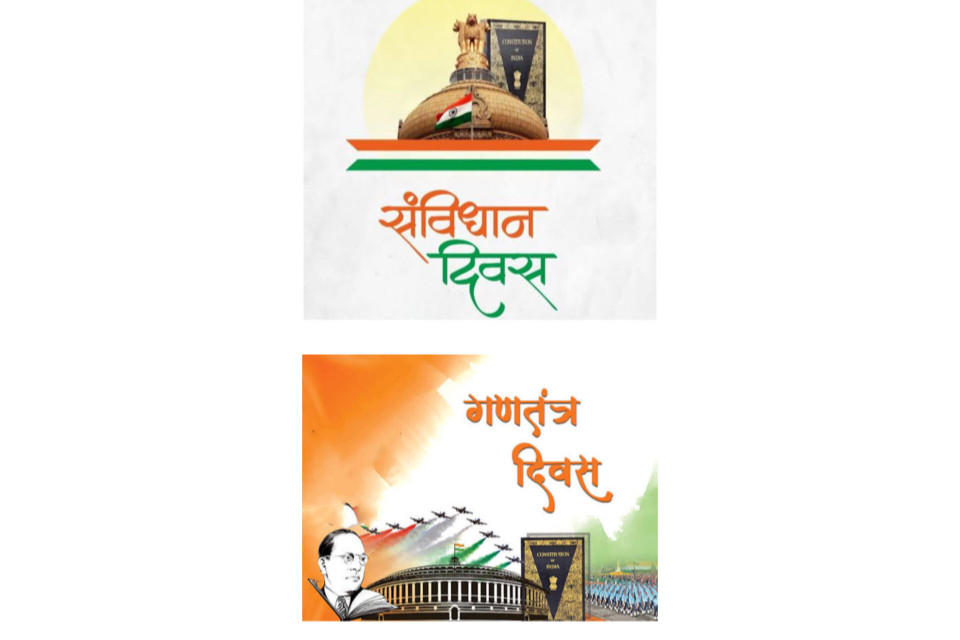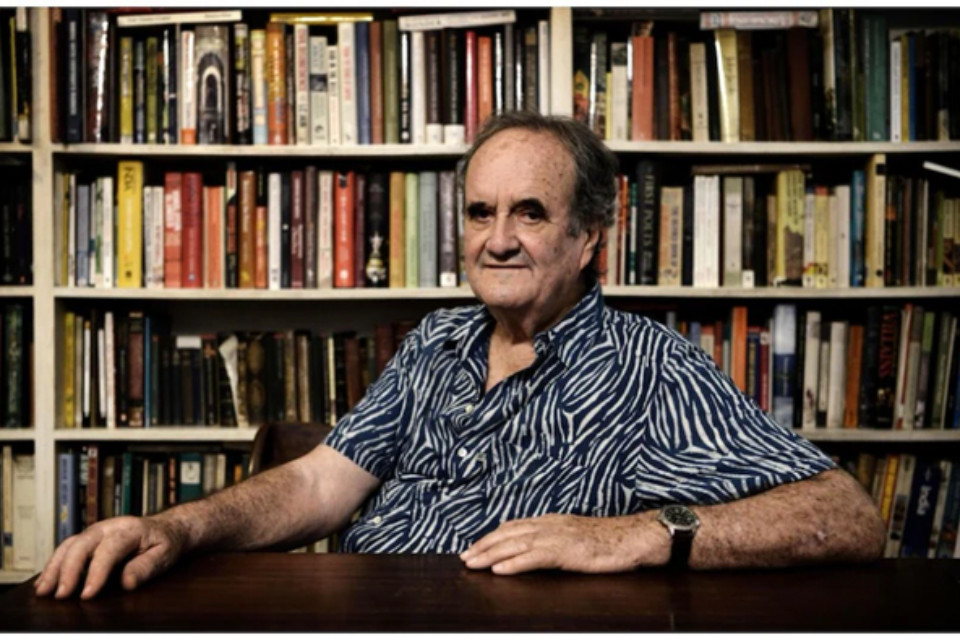चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवालः आधार हर जगह जरूरी, मगर मतदाता पहचान में नहीं! आखिर दोहरे मापदंड क्यों?

-सुनील मेहता-
भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर टिकी है और इसकी जिम्मेदारी संवैधानिक संस्था भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर है। लेकिन हाल के वर्षों में, विशेषकर 2025 में, आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि क्या वोटरों की मां-बेटियों के सीसीटीवी फुटेज साझा करने चाहिए? ने न केवल विवाद को जन्म दिया, बल्कि आयोग की जवाबदेही पर भी संदेह पैदा किया है। यह बयान, जो विपक्षी नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के जवाब में आया, न सिर्फ संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है, बल्कि मतदाताओं की गोपनीयता के नाम पर पारदर्शिता से बचने की कोशिश को भी उजागर करता है। राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका के बोस्टन में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि शाम 5ः30 से 7ः30 बजे के बीच 65 लाख लोगों ने वोट डाला, जो शारीरिक रूप से असंभव है। उनकी यह टिप्पणी, जो मतदाता डेटा में विसंगतियों की ओर इशारा करती है,
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी है, जहां आयोग ने 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मिलकर मसौदा सूची तैयार की। लेकिन आयोग का यह दावा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी थी, विपक्ष के आरोपों और जनता के बीच बढ़ते अविश्वास के सामने कमजोर पड़ता है। खासकर, जब आयोग ने सीसीटीवी फुटेज साझा करने से इनकार किया और आधार कार्ड को मतदाता पहचान के लिए मान्यता देने से मना किया, तो यह संदेह और गहरा हो गया। आधार, जिसे सरकार ने अन्य क्षेत्रों में अनिवार्य बनाया, को चुनाव प्रक्रिया में खारिज करना पारदर्शिता के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। चुनाव आयोग का कहना है कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का उद्देश्य डुप्लिकेट मतदाताओं को रोकना है, जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के संशोधन में सुझाया गया। लेकिन इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और सीसीटीवी फुटेज जैसे ठोस सबूतों को साझा न करना जनता के बीच अविश्वास को बढ़ावा दे रहा है।
बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष के सवाल और आंकड़ों में कथित गड़बड़ियां इस बात का संकेत हैं कि निष्पक्ष चुनावों की गारंटी अब उतनी मजबूत नहीं रही। इन विवादों का असर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर गहरा हो सकता है। यदि जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से उठता है, तो मतदान में भागीदारी कम हो सकती है, और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। पहले से ही, राजनीतिक दलों और शक्तिशाली हित समूहों के दबाव ने आयोग की स्वायत्तता को चुनौती दी है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम बनाया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और अन्य शामिल हों, ताकि आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित हो। लेकिन इस सिफारिश को लागू न करना आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। विश्व पटल पर भारत की स्थिति भी इस संदर्भ में प्रभावित हो रही है। एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों ने मजबूती दी थी, लेकिन हाल के विवादों ने इसे कमजोर किया है।
अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक और संगठन, जैसे फ्रीडम हाउस, पहले ही भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों पर बढ़ते दबाव की ओर इशारा कर चुके हैं। यदि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे, तो भारत का वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक प्रभावित हो सकता है, जो विदेशी निवेश और कूटनीतिक रिश्तों पर असर डाल सकता है। आने वाले समय में, यदि आयोग अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं लाता और जनता के सवालों का जवाब नहीं देता, तो भारत के लोकतंत्र पर गंभीर संकट आ सकता है। मतदाता सूची में सुधार, सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता और आधार जैसे पहचान पत्रों को मान्यता देना जैसे कदम न केवल आयोग की विश्वसनीयता को बहाल कर सकते हैं, बल्कि जनता का भरोसा भी जीत सकते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग न सिर्फ निष्पक्ष हो, बल्कि निष्पक्ष दिखे भी।